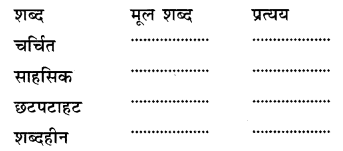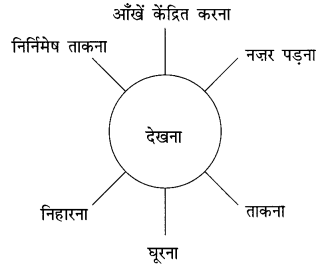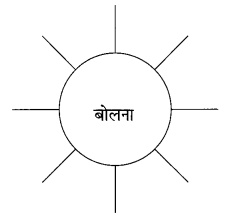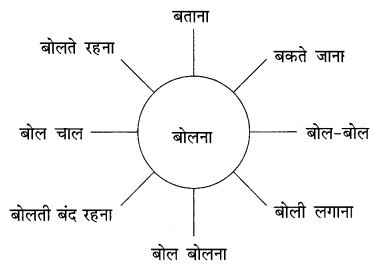NCERT Solutions (हल प्रश्नोत्तर)
तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र : प्रहलाद अग्रवाल (कक्षा-10 पाठ-11 हिंदी स्पर्श 2)
TEESREE KASAM KE SHILPKAR SHAILENDRA : Prahlad Aggrawal (Class-10 Chapter-11 Hindi Sparsh 2)
तीसरी कसम की शिल्पकार शैलेंद्र – प्रहलाद अग्रवाल
पाठ के बारे में…
यह पाठ ‘तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र’ प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखा गया एक पाठ है, जिसमें उन्होंने गीतकार शैलेंद्र के बारे में वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हिंदी फिल्म जगत में सार्थक और उद्देश्य पर फिल्म बनाना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम है।
‘तीसरी कसम’ फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। वे लंबे समय से कवि और हिंदी फिल्मों के गीतकार के रूप में हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम बनाए हुए थे। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ‘मारे गए गुलफाम’ को तीसरी कसम के नाम से सिनेमा के पर्दे पर उतारा था। यह फिल्म हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और हिंदी फिल्म की अमर कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने तीसरी कसम के निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन किया है।
लेखक के बारे में…
प्रहलाद अग्रवाल, जिनका जन्म मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में सन 1947 में हुआ था, वह हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों पर काफी कुछ लिखा है।
उनकी प्रमुख कृतियों में सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर आधी : हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र : जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा : चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग : सुभाष गई, ओ रे मांझी : विमल गाय का सिनेमा, महा बाजार के नायक : 21वीं सदी का सिनेमा आदि के नाम प्रमुख हैं।
हल प्रश्नोत्तर
मौखिक
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो पंक्तियों में दीजिए-
प्रश्न 1 : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म को कौन-कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
उत्तर : ‘तीसरी कसम’ फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
- तीसरी कसम फिल्म को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा ‘राष्ट्रपति स्वर्ण पदक’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- ‘तीसरी कसम’ फिल्म को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
- ‘तीसरी कसम’ इनको मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा तीसरी कसम फिल्म को अन्य कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
तीसरी कसम फिल्म कवि-गीतकार शैलेंद्र द्वारा निर्मित एक हिंदी फिल्म थी, जिसमें मुख्य भूमिका राज कपूर और वहीदा रहमान ने निभाई थी। ये फिल्म प्रसिद्ध हिंदी लेखक नाथ रेणु के उपन्यास ‘मारे गए गुलफाम’ पर आधारित थी।
प्रश्न 2 : शैलेंद्र ने कितनी फ़िल्में बनाई?
उत्तर : शैलेंद्र ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम ‘तीसरी कसम’ था।शैलेंद्र हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अनेक अनमोल गीत लिखे।
‘तीसरी कसम’ फिल्म के मुख्य कलाकारों में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज कपूर और अभिनेत्री वहीदा रहमान थी। यह फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए उपन्यास ‘मारे गए गुलफाम’ पर आधारित थी। यह फिल्म हिंदी फिल्म जगत की अमर कलाकृति में से एक मानी जाती है।
प्रश्न 3 : राजकपूर द्वारा निर्देशित कुछ फ़िल्मों के नाम बताइए।
उत्तर : राजकपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं…
मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, जागते रहो, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, कल आज और कल, बॉबी।
राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के एक जाने-माने निर्माता-निर्देशक थे। जिन्हें हिंदी फिल्म जगत में ‘शोमैन’ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फिल्में बेहद भव्य एवं विशाल कैनवास पर बनाई गई हुई होती थीं, और उनकी फिल्में अपार लोकप्रियता प्राप्त करती थी।
राज कपूर के साथ गीतकार शैलेंद्र, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर-जयकिशन इन पाँचों की जुगलबंदी उस समय हिंदी फिल्म जगत में बेहद प्रसिद्ध थी।
प्रश्न 4 : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फ़िल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है?
उत्तर : कसम फिल्म के नायक और नायिकाओं के नाम इस प्रकार हैं…
नायक : राजकपूर नायिका : वहीदा रहमान
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज कपूर ने इस फिल्म में ‘हीरामन’ नामक एक गाड़ीवान की भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान ने इस फिल्म में नौटंकी कलाकार ‘हीराबाई’ की भूमिका निभाई थी। इन फिल्म इन दोनों के बीच घटे प्रसंगों पर आधारित थी, जोकि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ‘मारे गये गुलफाम’ के कथानक पर हुई है।
प्रश्न 5 : फ़िल्म ‘तीसरी कसम’ का निर्माण किसने किया था?
उत्तर : ‘तीसरी कसम’ फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। शैलेंद्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। उन्होंने अनेक हिंदी फिल्मों के लिए अनेक अनमोल गीतों की रचना की है। राज कपूर के साथ उनकी जुगलबंदी प्रसिद्ध थी और उन्होंने राज कपूर की लगभग सभी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं।
‘तीसरी कसम’ फिल्म का निर्माण करते समय उन्होंने राज कपूर को ही मुख्य अभिनेता चुना था और फिल्म की अभिनेत्री वहीदा रहमान थी। तीसरी कसम फिल्म का निर्माण 1966 में हुआ था और इस फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था।
प्रश्न 6 : राजकपूर ने ‘मेरा नाम जोकर’ के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी?
उत्तर : राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की जरा भी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें इस फिल्म के निर्माण में इसका एक भाग बनाने में ही 6 साल का लंबा समय लग जाएगा।
राज कपूर को मेरा नाम फिल्म के निर्माण के समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अनेक तरह की मुश्किल परिस्थितियों से निभाते हुए एक लंबे समय में मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म के निर्माण ने आर्थिक रूप से काफी कमजोर कर दिया था और उन पर काफी कर्जा चढ़ गया था।
प्रश्न 7: राजकपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया?
उत्तर : राजकपूर की इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया कि जब राजकपूर ने ‘तीसरी कसम’ फिल्म में अपने अभिनय के लिए उनसे मेहनताना मांगा तो गीतकार शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया।
शैलेंद्र और राज कपूर आपस में घनिष्ठ मित्र थे। राजकपूर की लगभग सभी फिल्मों के लिए शैलेंद्र ने गीत लिखे थे। जब शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण आरंभ किया तो उन्हें उम्मीद थी कि राज कपूर दोस्ती के नाते बिना किसी मेहनताने में काम करना स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्हें आर्थिक रूप से काफी परेशानी उठानी पड़ी थी।
लेकिन जब एक दिन राजकपूर ने फिल्म में अपने काम के लिए मेहनताना मांगा तो शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्हें ऐसी आशा ना थी। लेकिन जब राज कपूर ने तुरंत ही उनसे मुस्कुराते हुए मेहनताने के रूप में केवल 1 रुपये की मांग की, शैलेंद्र को सारी बात समझ में आई और राज कपूर ने वास्तव में उनसे दोस्ती निभाई थी।
प्रश्न 8 : फ़िल्म समीक्षक राजकपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे?
उत्तर : फिल्म समीक्षक राजकपूर को कला मर्मज्ञ और आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे।विस्तार से कला मर्मज्ञ से तात्पर्य कला का पारखी, जिसे कला के विषय में पूर्ण ज्ञान हो और जो एक नजर में ही सही आकलन कर लेता हो।
राजकपूर आँखों से बात करने की कला भी जानते थे और वह आँखों में ही आँखों मैं अपनी बात कह जाते थे और समझ जाते थे। वह फिल्मों में अपनी आँखों के भाव प्रदर्शन से ही बिना संवाद बोले ही अपनी बात कह जाते थे। इसलिए फिल्म समीक्षक राजकपूर को कला मर्मज्ञ और आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे।
लिखित
(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर (25-30 शब्दों में) लिखिए-
प्रश्न 1 : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म को ‘सैल्यूलाइड पर लिखी कविता’ क्यों कहा गया है?
उत्तर : तीसरी कसम’ फिल्म को सेल्यूलाइड पर उतरी कविता इसलिए कहा गया था क्योंकि यह फिल्म सेल्यूलाइड पर कविता जैसी अनुभूति प्रदान करती थी। सेल्यूलाइड से तात्पर्य कैमरे की रील पर फिल्म को उतारने से होता है।तीसरी कसम फिल्म ग्रामीण जीवन के मार्मिक प्रसंगों को समेटती हुई एक ऐसी भाव प्रणव कहानी थी, जो बिल्कुल काव्यात्मकता का अनुभूति कराती थी।
फिल्म को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सेटेलाइट पर कोई कविता चल रही हो। इस फिल्म में नायक और नायिका का सहज एवं भावपूर्ण अभिनय फिल्म में एक अलग ही अनुभूति उत्पन्न करता है। इसी कारण इस फिल्म को सेल्यूलाइड लिखी गई कविता कहा गया है।
प्रश्न 2 : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म को खरीददार क्यों नहीं मिल रहे थे?
उत्तर : तीसरी कसम’ फिल्म को खरीदार इसलिए नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यह फिल्म एक साहित्यिक कृति पर आधारित भाव प्रधान फिल्म थी, जिसमें साहित्यिकता और कलात्मकता का संगम था। फिल्मकार ने फिल्म की विषय वस्तु और कथानक से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था। यह एक कलात्मक कृति थी, जिसमें व्यवसायिकता का पुट जरा भी नहीं था।
फिल्म के खरीदार फिल्म को मुनाफे का सौदा मान कर ही खरीदते हैं और उन्हें ये फिल्म में व्यवसायिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं दिख रही थी। इसीलिए इस फिल्म को खरीदा नहीं मिले । लेकिन बाद में इसी फिल्म ने इतिहास रचा और यह फिल्म हिंदी फिल्म जगत की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक मानी जाती है।
प्रश्न 3 : शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है?
उत्तर : शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह दर्शकों की रुचि के अनुसार अपनी कला को प्रदर्शित करें। कलाकार अपने वह दर्शकों/श्रोताओं की रुचि को परिष्कृत करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करें ना कि उनको सस्ता एवं भौंडा मनोरंजन उन पर थोपने का प्रयत्न करें। कलाकार का मुख्य कर्तव्य कला के शुद्ध एवं सात्विक रूप को समाज के सामने प्रस्तुत कर सुंदर एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना होता है।
कलाकार को अपनी कला को विकृत नहीं करना चाहिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से कला को सस्ते रूप में नहीं प्रदर्शित करना चाहिए।
प्रश्न 4 : फ़िल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरिफाई क्यों कर दिया जाता है?
उत्तर : फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरिफाई इसलिए कर दिया जाता है ताकि फिल्म निर्माता अपने व्यवसाय उद्देश्यों को साथ कर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। फिल्म में त्रासद स्थितियों का ग्लोरिफाई करके दर्शकों की भावनाओं को उत्तेजित किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक दर्शक फिल्म देखने को आएं और निर्माताओं को अधिक से अधिक कमाई हो ।
त्रासद स्थितियों का ग्लोरिफाई करके दर्शकों की भावनाओं से खेला जाता है। ये दर्शकों को फिल्म की ओर खींचने की एक व्यवसायिक रणनीति होती है। वास्तविक जीवन में ऐसी त्रासद स्थितियां नही होती जैसी फिल्म में दिखाईं जाती हैं, फिल्म में उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है।
प्रश्न 5 : ‘शैलेंद्र ने राजकपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं’- इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर : शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं दिए हैं। इस कथन का आशय यह है कि तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर में बेहद तन्मयता से अभिनय किया था। राज कपूर अपनी आँखों से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। वे आँखों ही आँखों में अपनी भावना व्यक्त कर इतना भावपूर्ण अभिनय करते थे कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था।
शैलेंद्र राज कपूर के गीतकार रहे हैं उन्होंने अपने गीतों के शब्दों के माध्यम से राज कपूर की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया था। इस फिल्म के गीत भी एक से एक अधिक जानदार थे जो कि शैलेंद्र द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म गीतों के बोलों को राज कपूर ने अपने भावपूर्ण अभिनय से जीवंत कर दिया था। इसीलिए यह कथन बिल्कुल कहना ठीक है कि शैलेंद्र ने ही राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए।
प्रश्न 6 : लेखक ने राजकपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर : लेखक ने राजकपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शौमैन से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जिसमें अपने कला के प्रदर्शन द्वारा एक बड़े विशाल जनसमुदाय को आकर्षित करने की क्षमता हो। जिसकी कला का कायल एक विशाल जन वर्ग हो।
राजकपूर एक ऐसे ही आकर्षक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी कलाकारी गुण से हिंदी सिनेमा जगत को अनेक अनोखी फिल्में प्रदान कीं। उनकी फिल्में बेहद लोकप्रिय होती थी और लोगों के दिल में एक अलग जगह बना लेती थी। उनकी फिल्में ना केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब लोकप्रिय होती थी।
लोग उनके नाम से ही फिल्में देखने जाया करते थे। वह केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक निर्माता सफल निर्माता और सफल निर्देशक भी थे। अभिनेता के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने निर्देशन के रूप में एक से एक शानदार फिल्में दें और बेहद लोकप्रियता अर्जित की जिनमें राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, बॉबी जैसी फिल्मों के नाम प्रसिद्ध है।
राज कपूर की फिल्में भारत में ही नहीं रूस में बेहद लोकप्रिय होती थीं। वे रूस में बेहद लोकप्रिय थे। पूरे एशिया में जितने विशाल स्तर पर किसी प्रकार की फिल्में नहीं लोकप्रिय होती थीं, जितनी की राजकपूर की फिल्में होती थीं। इसीलिए उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन में कहा गया है।
प्रश्न 7 : फ़िल्म ‘श्री 420′ के गीत ‘रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ’ पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों की?
उत्तर : फिल्म ‘श्री 420’ के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीता जयकिशन ने आपत्ति इसलिए की, क्योंकि संगीतकार जयकिशन के अनुसार सामान्यजन इतनी गूढ़ बातों को नहीं समझ सकता। सामान्यजन केवल चार दिशाओं के बारे में जानता है।
गहन विस्तार में जाएं तो दसों दिशाएं भी होती हैं, लेकिन सामान्यजन इस बारे में नहीं जानता इसलिए सामान्य जन केवल चार दिशाओं को समझेगा जो उसकी जनसामान्य सोच के अंतर्गत आता है। वह दसों दिशाओं वाली साहित्यिक सोच के संदर्भ को समझ नहीं पाएगा। इसलिए शंकर जयकिशन को श्री 420 के गीत ‘रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां’ पर आपत्ति थी।
शैलेंद्र इस बात के लिए तैयार नही हुए, अपने अपने गीत को सस्ता नही बनाना चाहते थे इसलिए गीत के शब्द ज्यों के त्यों रहे।
(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर (50-60 शब्दों में) लिखिए-
प्रश्न 1 : राजकपूर द्वारा फ़िल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फ़िल्म क्यों बनाई?
उत्तर : राजकपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि वह इस फिल्म के माध्यम से अपने कलाकार मन को आत्म संतुष्टि देना चाहते थे। शैलेंद्र एक भागवत कवि हृदय कलाकार थे।
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए ‘मारे गए गुलफाम’ उपन्यास का कथानक उनके मन को छू गया था। इसी कारण वह इस पर एक फिल्म बनाकर अपने कलाकार मन को संतुष्टि देना चाहते थे। यूं तो वह काफी समय से फिल्म जगत में थे लेकिन उनका फिल्म बनाने का उद्देश्य व्यवसायिक नही था बल्कि वह अपने कलाकार मन की भावनाओं को फिल्मी पर्दे पर उकेरना चाहते थे।
चूँकि फिल्म बनाने का उनका उद्देश्य व्यवसायिक नही था, इसीलिए राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई।
प्रश्न 2 : ‘तीसरी कसम’ में राजकपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर : राजकपूर एक बेहद मंजे हुए कलाकार थे। वह जिस किसी भी किरदार को निभाते थे तो उस पर अपने व्यक्तित्व को हावी नहीं होने देते थे, बल्कि वे उस पर किरदार अपने अंदर आत्मसात कर लेते थे। पर्दे पर उनके द्वारा निभाया गया किरदार वो किरदार ही लगता था, उसमें राज कपूर कहीं भी नजर नहीं आता था। हीरामन के किरदार के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया।
हीरामन एक देहाती व्यक्तित्व वाला किरदार था, जिसको निभाने के लिए राज कपूर ने पूरा देहाती अंदाज अपना लिया था। हीरामन उकड़ूं बैठता है और बातें देहाती अंदाज में करता है तथा ग्रामीण व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह सारे गुण उन्होंने हीरामन के किरदार में भर दिए थे।
फिल्म देखते समय उनके किरदार को देखते हुए राज कपूर कहीं भी नहीं दिखाई देते बल्कि उसमें हीरामन ही नजर आता था। इस तरह उनके द्वारा किया गया जीवंत अभिनय हीरामन की आत्मा में उतर गया था।
प्रश्न 3 : लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि ‘तीसरी कसम’ ने साहित्य-रचना के साथ शत-प्रतिशत न्याय किया है?
उत्तर : लेखक ने ऐसा इसलिए लिखा है कि तीसरी कसम में साहित्य रचना के साथ शत-प्रतिश न्याय किया गया है, क्योंकि शैलेंद्र ने फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म की मूल कथा से जरा भी छेड़छाड़ नहीं की थी। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास ‘मारे गए गुलफाम’ के कथानक के आधार पर किया था।
उन्होंने मूल कहानी के स्वरूप में जरा भी बदलाव नहीं किया है। शैलेंद्र ने कहानी के सभी पात्रों को यथावत उसी रूप में प्रस्तुत किया है, जिस रूप में उपन्यास में उनका वर्णन किया गया है। उन्होंने ग्रामीण जीवन और उनके पात्रों तथा उनकी बोली को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है और पूरी फिल्म एक साहित्य कृति बन गई है। उन्होंने इस फिल्म में ग्रामीण जीवन का सटीक चित्रण किया है।
कहने को इस फिल्म में उस समय के बड़े-बड़े कलाकार जैसे राजकपूर और वहीदा रहमान ने काम किया था लेकिन किसी भी कलाकार का व्यक्तित्व किरदार पर हावी नहीं हुआ है। फिल्म के गीत संगीत भी ग्रामीण जीवन की लोकगीतों पर ही आधारित है। इसीलिए लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य के साथ शत-प्रतिशत न्याय किया है।
प्रश्न 4 : शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर : शैलेद्र के गीतों की मुख्य विशेषता यह होती थी कि उनके गीत सरल और सहज भाषा में रचित होते थे। शैलेंद्र अपने गीतों में बेहद कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि जनसाधारण की समझ में आ जाने वाले सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण होते थे और उनके गीतों में करुणा, संवेदना जैसे भाव भरे होते थे।
वे आम जनमानस के जीवन से जुड़े होते थे। शैलेंद्र के गीतों में अभिजात्य वर्ग का झूठा पाखंड नहीं होता था। उनके गीत आम जनमानस के अधिक निकट होते थे, जो दिल की गहराइयों को छू लेते थे।
प्रश्न 5 : फ़िल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर : फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र ने अपने जीवन में ‘तीसरी कसम’ नाम की केवल एक ही फिल्म बनाई थी। लेकिन इस फिल्म के साथ उन्होंने निर्माता के रूप में पूरा न्याय किया था। उन्होंने फिल्म की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया था। ये फिल्म एक साहित्यिक कृति पर आधारित थी और शैलेंद्र स्वयं साहित्य से संबंध रखते थे।
शैलेंद्र एक कवि-गीतकार थे और उनका कवि हृदय व कलाकार मन किसी भी साहित्यिक कृति के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। शैलेंद्र ने ये फिल्म धन कमाने की लालसा स नही नहीं बनाई थी, इसलिए व्यवसाय की दृष्टि से भले ही अच्छे निर्माता नहीं हो पाए लेकिन कलात्मकता और गुणवत्ता की दृष्टि से उन्होंने एक उत्कृष्ट फिल्म का निर्माण किया था। उन्होंने जिस साहित्यिक कृति पर इस फिल्म का निर्माण किया था उसे यथावत पर्दे पर पेश किया।
उन्होंने कहानी के दो मुख्य पात्रों हीरामन और हीराबाई के पवित्र प्रेम को बेहद संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारा था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया और । इसी कारण उन्होंने एक अनमोल और अमर कलाकृति वाली फिल्म बनाई।
प्रश्न 6 : शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फ़िल्म में झलकती है-कैसे? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर : शैलेंद्र एक सीधे सच्चे सरल व्यक्ति थे। वे एक कवि और गीतकार होने के कारण एक कोमल हृदय वाले कलाकार थे। उनका जीवन सादा एवं सरल होता था और अपने निजी जीवन को वह अपने गीतों के माध्यम से भी प्रकट करते थे। अपने गीतों में उन्होंने कभी भी झूठे अभिजात्य को नहीं अपनाया बल्कि आम जनमानस की भावनाओं को अधिक उभारा है।
शैलेंद्र के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि उनके गीतों में झूठा प्रदर्शन नहीं होता था बल्कि वह आम जनजीवन की विसंगतियों को बताते थे। उनके गीत की भाषा सरल एवं सहज होती थी इसका मुख्य कारण यह था वह भी स्वयं सच्चे सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके निजी जीवन की विशेषता थी और अपनी इसी विशेषता को उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से फिल्में भी प्रकट किया है। जिस तरह तीसरी कसम फिल्म में उन्होंने फिल्म के मुख्य नायक हीरामन को दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, वैसे ही शैलेंद्र भी स्वयं फिल्म जगत में रहते हुए भी फिल्म जगत की चकाचौंध से दूर सीधे एवं सरल रूप से रहते थे।
फिल्म का निर्माण में भी उन्हें अनेक संघर्षों और कठिनाइयों पड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नही मानी और फिल्म का निर्माण करके ही दम लिया। यही बात उन्होंने अपनी फिल्म के नायक और गीतों से भी प्रकट की है। इस तरह उनके निजी जीवन की छाप उनके फिल्म में झलकती है।
प्रश्न 7 : लेखक के इस कथन से कि ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म कोई सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर : लेखक के इस कथन से कि ‘तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था।’ पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। शैलेंद्र ने इस फिल्म का निर्माण करते समय जिस तरह की संवेदनशीलता और भावप्रणवता दिखाई है, वह कोई कवि हृदय ही दिखा सकता था।
फिल्म के सभी पात्रों में संवेदनशीलता, करुणा आदि का भाव प्रकट होता है। उन्होंने फिल्म के नायक और नायिका के मनोभावों को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है जो कि एक कवि हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता था। उन्होंने पूरी फिल्म में संवेदनशीलता तथा भावनात्मकता का ध्यान रखा है। कोई आम फिल्म निर्माता फिल्म के व्यवसायिक पक्षों को भी ध्यान में रखता और फिल्म में कल्पना और अतिशयोक्ति वाले दृश्यों का समावेश कर सकता था, लेकिन शैलेंद्र ने ऐसा नहीं किया उन्होंने मूल साहित्य कृति के यथावत बरकरार रखा और फिल्म को वास्तविकता के अधिक निकट दिखाया है।
ये सारे कार्य के कवि हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है कि ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म कोई सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था।
(ग) निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए-
प्रश्न 1 : …. वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी।
आशय : वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म-संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी।आशय : इन पंक्तियों का आशय यह है कि शैलेंद्र एक ऐसे भावुक कवि थे, जिन्हें धन और यश की कामना नहीं थी। वह अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ही कार्य करते थे। इसी कारण उन्होंने जब तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया तो उस फिल्म का निर्माण उन्होंने धन की लालसा से नहीं किया था बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए किया था।
तीसरी कसम फिल्म जिस साहित्य कृति पर आधारित करके उन्होंने बनाई थी वह साहित्य कृति उनके मन को बेहद भा गई थी और वह इसे फिल्मी पर्दे पर उतारना चाहते थे। उन्हें फिल्म की असफलता के खतरे से आगाह भी किया गया था लेकिन उन्हें तो धन-संपत्ति और यश की कामना ही नहीं थी उन्हें तो अपने कलाकार मन को संतुष्ट करना था।
इसीलिए सारी बातों को परे रखकर इतनी सुंदर और अनुपम फिल्म का निर्माण किया, ऐसा तो एक भावुक कवि हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता था।
प्रश्न 2 : उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे।
आशय : इस पंक्ति का यह आशय है कि कवि शैलेंद्र का मानना था कि एक कलाकार को दर्शकों की अभिरूचि की आड़ के बहाने अपनी कला को विकृत नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर जबरदस्ती कुछ ऐसा थोपना चाहिए। जब श्री 420 फिल्म एक गाना बनाया जा रहा था तो शैलेंद्र ने उस गीत में दसों दिशाओं शब्द का प्रयोग किया था।
तब संगीतकार जयकिशन ने इस शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा कि दसों दिशाओं शब्द आम शब्द नहीं है और इसे आम जनमानस नहीं समझता। लोग केवल चार दिशाएं जानते हैं, दस दिशाएं नहीं। इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। परंतु शैलेंद्र ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमेशा दर्शकों की रूचि के बहाने हमें अपनी कला को विकृत नहीं करना चाहिए। भले ही लोग दशों दिशा नहीं जानते लेकिन गीत में आने पर उसे जानने लगेंगे।
यदि हम अपने गीतों के माध्यम से सही बात रखेंगे तो दर्शक अवश्य समझेंगे। कलाकार दर्शकों के प्रभाव में आकर गलत बातों को प्रोत्साहित करने लगते हैं, जिससे फिर कला में विकृतता आज आ जाती है। एक कलाकार का मुख्य कर्तव्य होता है कि वह दर्शक, श्रोता की रूचियों का परिष्कार करें यानी उनकी रूचियों को सुधारें और सही बात को सही ढंग से प्रस्तुत करें।
प्रश्न 3 : व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है।
आशय : इन पंक्तियों का आशय यह है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमारे जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां और विपत्तियां आती हैं, जिनका सामना करना चाहिए। जब भी कोई कठिनाई विपत्ति आदि आती है तो वह उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगता है और कुछ ना कुछ ऐसा प्रयत्न करता है कि उसे उस संकट से मुक्ति मिले। इसलिए जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से जुड़कर ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है।
जिंदगी में आने वाली कठिनाइयां हमें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती हैं और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। मनोबल मजबूत होने पर और संघर्ष करने की क्षमता से ही जिंदगी में सफलता पाई जा सकती है, इसलिए कठिनाई आने पर उनसे न घबराकर उनका सामना करना चाहिए।
प्रश्न 4 : दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने वाले की समझ से परे है।
आशय : इस पंक्ति का आशय यह है कि शैलेंद्र ने तीसरी कसम नाम की जो फिल्म बनाई थी, वह व्यवसायिक फिल्म नहीं थी। इसलिए वे निर्माता लोग जो फिल्म बनाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह फिल्म उनकी समझ से परे थी। शैलेंद्र ने यह फिल्म अपने संवेदनशील कवि मन की आत्म संतुष्टि कथा एक साहित्यिक कृति का सही संदेश देने के लिए फिल्म बनाई थी।
इस फिल्में व्यवसायिकता समावेश नहीं था बल्कि कलात्मकता और साहित्यिकता का समावेश था। इसलिए फिल्म के नाम पर व्यापार करने वालों के लिए यह फिल्म किसी काम की नहीं थी । यही कारण था कि जब इस फिल्म को आसानी से खरीदार नही मिले थे। बाद में इसी फिल्म में हिंदी फिल्म जगह में एक अनमोल कृति के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है।
प्रश्न 5 : उनके गीत भाव-प्रवण थे- दुरूह नहीं।
आशय : इस पंक्ति का आशय यह है कि कभी शैलेंद्र जो भी बेचते थे वह भावनाओं से भरे हुए होते थे। उनके गीतों में आम जनमानस की भावना एवं संवेदना प्रकट होती थी। उनके गीतों की भाषा सरल एवं सहज होती थी, जो किसी भी आम व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती थी। इसीलिए उनके गीतों को समझना कोई कठिन बात नहीं थी। यही कारण था उनके गीत हर किसी के मन की को गहराई तक छू जाते थे और बेहद लोकप्रिय होते थे।
भाषा अध्ययन
प्रश्न 1 : पाठ में आए ‘से’ के विभिन्न प्रयोगों से वाक्य की संरचना को समझिए।
राजकपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फ़िल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया।
रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ।
फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर-तरीकों से नावाकिफ़ थे।
दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने के गणित जानने वाले की समझ से परे थी।
शैलेंद्र राजकपूर की इस याराना दोस्ती से परिचित तो थे।
उत्तर : वाक्यों में ‘से’ के विभिन्न प्रयोगों से वाक्य की संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है।
1. राजकपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फ़िल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया।
➲ यहाँ ‘से’ का प्रयोग हैसियत के संदर्भ में किया गया है। यह बताता है कि राजकपूर ने एक मित्र के रूप में शैलेंद्र को चेताया।
2. रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ।
➲ यहाँ ‘से’ का प्रयोग स्थान के स्रोत के रूप में किया गया है। यह दर्शाता है कि रातें सभी दिशाओं से कहानियाँ सुनाएंगी।
3. फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर-तरीकों से नावाकिफ़ थे।
➲ यहाँ ‘से’ का प्रयोग तौर-तरीकों के संदर्भ में किया गया है। यह बताता है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के तौर-तरीकों से अनजान थे।
4. दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने के गणित जानने वाले की समझ से परे थी।
➲ यहाँ ‘से’ का प्रयोग तुलना और सीमा के संदर्भ में किया गया है। यह दर्शाता है कि इस फिल्म की संवेदना उस व्यक्ति की समझ से परे थी जो केवल लाभ की गणना जानता है।
5. शैलेंद्र राजकपूर की इस याराना दोस्ती से परिचित तो थे।
➲ यहाँ ‘से’ का प्रयोग संबंध और कारण के रूप में किया गया है। यह बताता है कि शैलेंद्र राजकपूर की दोस्ती से परिचित थे।
इस प्रकार, ‘से’ का प्रयोग अलग-अलग संदर्भों में किया गया है जैसे हैसियत, स्रोत, तौर-तरीकों, तुलना, और संबंध, जो वाक्य की संरचना और अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं।
प्रश्न 2 : इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों की संरचना पर ध्यान दीजिए-
‘तीसरी कसम’ फ़िल्म नहीं, सैल्यूलाइड पर लिखी कविता थी।
उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था।
फ़िल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा।
खालिस देहाती भुच्चे गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं।
उत्तर : आइए की इन वाक्यों की संरचना को समझते हैं…
1. ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म नहीं, सैल्यूलाइड पर लिखी कविता थी।
संरचना : यह एक वर्णनात्मक वाक्य है जिसमें ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म की तुलना सैल्यूलाइड पर लिखी कविता से की गई है। इसमें ‘नहीं’ का प्रयोग नकारात्मकता को इंगित करता है और ‘थी’ का प्रयोग वाक्य को पूर्ण करता है।
• विषय : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म
• क्रिया : नहीं थी
• वस्तु : सैल्यूलाइड पर लिखी कविता
2. उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था।
संरचना : यह एक संयोजक वाक्य है जिसमें दो विचारों को जोड़ने के लिए ‘जिसे’ और ‘ही’ का प्रयोग किया गया है। इसमें ‘उन्होंने’ कर्ता (doer) है, और ‘ऐसी फ़िल्म’ कर्म है।
• विषय : उन्होंने
• क्रिया : बनाई थी
• वस्तु : ऐसी फ़िल्म
• पूरक : जिसे सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था
3. फ़िल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा।
संरचना : यह एक समन्वय वाक्य है जिसमें दो घटनाओं (फ़िल्म का आना और जाना) को जोड़कर निष्कर्ष (मालूम नहीं पड़ा) पर पहुँचाया गया है।
• विषय : फ़िल्म
• क्रिया : आई, चली गई
• पूरक : कब, मालूम ही नहीं पड़ा
4. खालिस देहाती भुच्चे गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं।
संरचना : यह एक विशेषणीय वाक्य है जिसमें ‘खालिस देहाती भुच्चे गाड़ीवान’ के गुणों का वर्णन किया गया है। वाक्य में ‘जो’ का प्रयोग संबंधबोधक है और ‘दिल की जुबान’ और ‘दिमाग की नहीं’ का प्रयोग तुलना के रूप में किया गया है।
• विषय : खालिस देहाती भुच्चे गाड़ीवान
• विशेषण : जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है
• विपर्यय : दिमाग की नहीं
इस प्रकार, इन वाक्यों की संरचना को समझकर यह ज्ञात होता है कि वाक्य कैसे बनाए गए हैं और उनके तत्व कैसे जुड़े हैं, जो पाठ की संपूर्णता और स्पष्टता में सहायक होते हैं।
प्रश्न 3 : पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए-
चेहरा मुरझाना, चक्कर खा जाना, दो से चार बनाना, आँखों से बोलना
उत्तर : मुहावरों पर वाक्य
चेहरा मुरझाना : जैसे राजू को पता चला कि वह परीक्षा में फेल हो गया है तो सुनते ही उसका चेहरा मुरझा गया।
चक्कर खा जाना : बाहर बहुत तेज धूप होने कारण राजू थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर पड़ा।
दो से चार बनाना : आजकल लालच और अंधी होड़ का युग है जिसमें लोग दो से चार बनाने में लगे रहते हैं।
आँखों से बोलना : उनका अभिनय इतना भाव प्रणव था कि वह आँखों से बोल काफी कुछ कह देते थे।
प्रश्न 4 : निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय दीजिए।
शिद्दत – …….
याराना – ……….
बमुश्किल – ………
खालिस – ………..
नावाकिफ़ – ……..
यकीन – …………
हावी – …………
रेशा – ……….
उत्तर : दिए गए शब्दों के पर्याय इस प्रकार होंगे..
निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय
1. शिद्दत – तीव्रता, गंभीरता
2. याराना – दोस्ती, मैत्री
3. बमुश्किल – कठिनाई से, मुश्किल से
4. खालिस – शुद्ध, निर्मल
5. नावाकिफ़ – अनजान, अपरिचित
6. यकीन – विश्वास, भरोसा
7. हावी – प्रभावशाली, नियंत्रित करने वाला
8. रेशा – तंतु, तागा
प्रश्न 5 : निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए-
चित्रांकन – ……… + ………
सर्वोत्कृष्ट – ………. + ………..
चर्मोत्कर्ष – ………… + ………….
रूपांतरण – ……….. + ………….
घनानंद – ………… + …………..
उत्तर : दिए शब्दों के संधि विच्छेद इस प्रकार होंगे…
- चित्रांकन : चित्र + अंकन
- सर्वोत्कृष्ट : सर्व + उत्कृष्ट
- चर्मोत्कर्ष : चरम + उत्कर्ष
- रूपांतरण : रूप + अंतरण
- घनानंद : घन + आनंद
प्रश्न 6 : निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए-
(क) कला-मर्मज्ञ
(ख) लोकप्रिय
(ग) राष्ट्रपति
उत्तर : समास विग्रह इस प्रकार होगा…
(क) कला-मर्मज्ञ : कला का मर्मज्ञ (संबंध तत्पुरुष समास)
(ख) लोकप्रिय : लोक में प्रिय (करण तत्पुरुष समास)
(ग) राष्ट्रपति : राष्ट्र का पति (संबंध तत्पुरुष समास)
योग्यता विस्तार
प्रश्न 1 : फणीश्वरनाथ रेणु की किस कहानी पर ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म आधारित है, जानकारी प्राप्त कीजिए और मूल रचना पढ़िए।
उत्तर : फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ‘मारे गए गुलफाम’ पर आधारित है फिल्म ‘तीसरी कसम’। यह कहानी एक ईमानदार और मासूम गाड़ीवान, हीरामन, और एक नाचने वाली, हीराबाई, की सरल और भावनात्मक प्रेम कहानी को प्रस्तुत करती है।
‘मारे गए गुलफाम’ कहानी का सारांश
मुख्य पात्र
1. हीरामन : एक सरल और ईमानदार गाड़ीवान, जिसकी दुनिया उसकी बैलगाड़ी और उसके बैल हैं।
2. हीराबाई : एक सुंदर और हृदयस्पर्शी नाचने वाली, जो मेलों और कार्यक्रमों में नृत्य करती है।
कहानी का सारांश
हीरामन की बैलगाड़ी में एक दिन हीराबाई सफर करती है। हीरामन, अपनी निर्दोष और सरल प्रकृति के कारण, हीराबाई के प्रति आकर्षित हो जाता है। हीराबाई की सुंदरता और उसके कोमल व्यवहार से प्रभावित होकर हीरामन उसे अपना दोस्त मान लेता है। कहानी के दौरान, हीरामन और हीराबाई के बीच एक मासूम और भावनात्मक रिश्ता विकसित होता है।
ये कहानी समाज की कठोर वास्तविकताओं और नैतिकताओं को उजागर करती है, जो हीराबाई जैसी नर्तकियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। अंततः, हीरामन को यह समझ में आता है कि वह हीराबाई को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा।
कहानी का अंत भावनात्मक और मार्मिक है, जब हीरामन हीराबाई से अलग हो जाता है, अपनी बैलगाड़ी में वापस लौटते हुए। इस अंत में एक गहरा संदेश छुपा है, जो प्रेम और समाज की वास्तविकताओं के बीच संघर्ष को दर्शाता है।
विद्यार्थी किसी भी नजदीकी पुस्तकालय में जाकर फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य खोजें। उनकी पुस्तकों में ये कहानी मिल जाएगी। वे फणीश्वरनाथ रेणु की किताबों में इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इस कहानी को भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसे कई भाषाओं में अनूदित भी किया गया है।
विद्यार्थी चाहें तो इसे साहित्यिक पुस्तकालयों, बुकस्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी खोज सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्यिक कार्यों का आनंद उठाने के लिए उनकी अन्य कहानियाँ और उपन्यास भी पढ़ सकते हैं।
प्रश्न 2 : समाचार पत्रों में फ़िल्मों की समीक्षा दी जाती है। किन्हीं तीन फ़िल्मों की समीक्षा पढ़िए और तीसरी कसम’ फ़िल्म को देखकर इस फ़िल्म की समीक्षा स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए।
उत्तर : ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म की समीक्षा इस प्रकार होगी..
फ़िल्म का नाम : तीसरी कसम
निर्देशक : बासु भट्टाचार्य
मुख्य कलाकार : राज कपूर, वहीदा रहमान
निर्माता : शैलेन्द्र
कहानी : फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ‘मारे गए गुलफाम’ पर आधारित
कहानी का सारांश
‘तीसरी कसम’ एक गहरी भावनात्मक और सामाजिक कथा है जो एक सरल और मासूम गाड़ीवान, हीरामन (राज कपूर), और एक सुंदर नाचने वाली, हीराबाई (वहीदा रहमान), के बीच के अनोखे रिश्ते को प्रस्तुत करती है। फिल्म बिहार के ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि में सेट है और भारतीय समाज की कठोर सच्चाइयों और नैतिकताओं को उजागर करती है।
राज कपूर ने हीरामन के किरदार में अपनी सरलता और मासूमियत को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया है। वहीदा रहमान ने हीराबाई के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है, उनकी आंखों की गहराई और भावनाओं ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री अद्वितीय है और उनकी परफॉर्मेंस ने कहानी को जीवंत बना दिया।
बासु भट्टाचार्य का निर्देशन सहज और संवेदनशील है। उन्होंने कहानी के हर पहलू को बहुत ही सुन्दरता से प्रस्तुत किया है। ग्रामीण जीवन की बारीकियों को जिस सजीवता से फिल्म में दर्शाया गया है, वह दर्शकों को बिहार की मिट्टी की खुशबू महसूस कराता है।
फ़िल्म का संगीत शंकर-जयकिशन द्वारा रचित है और गीत शैलेन्द्र द्वारा लिखे गए हैं। ‘सजन रे झूठ मत बोलो’ और ‘चलत मुसाफिर मोह लियो रे’ जैसे गीतों ने फिल्म को एक खास पहचान दी है। ये गीत कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं और फिल्म की भावना को और गहराई देते हैं।
फ़िल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा किया गया है, जो फिल्म के दृश्यों को बेहद खूबसूरत और वास्तविक बनाता है। ग्रामीण परिवेश, खेत-खलिहान, और मेलों की जीवंतता को बहुत ही प्रभावी तरीके से कैप्चर किया गया है।
संपादन में बासु भट्टाचार्य ने बहुत ही सटीकता से काम किया है। फिल्म का प्रवाह धीमा नहीं होता और दर्शक हर पल कहानी से जुड़े रहते हैं।
‘तीसरी कसम’ एक क्लासिक फिल्म है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि समाज की गहराइयों में जाकर सोचने पर मजबूर करती है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी और बासु भट्टाचार्य का निर्देशन इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं।
यह समीक्षा ‘तीसरी कसम’ की गहराई और सुंदरता को दर्शाने का एक प्रयास है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में अपनी अद्वितीयता और संवेदनशीलता के लिए हमेशा याद रखी जाएगी।
परियोजना कार्य
प्रश्न 1 : फ़िल्मों के संदर्भ में आपने अकसर यह सुना होगा-‘जो बात पहले की फ़िल्मों में थी, वह अब कहाँ’। वर्तमान दौर की फ़िल्मों और पहले की फ़िल्मों में क्या समानता और अंतर है? कक्षा में चर्चा कीजिए।
उत्तर : फिल्में समाज का दर्पण होती हैं और समय के साथ-साथ उनमें भी बदलाव आते रहते हैं। पहले की फिल्मों और वर्तमान दौर की फिल्मों में कई समानताएं और अंतर होते हैं। यहां उन पर एक नजर डालते हैं:
समानताएं
1. कहानी की महत्ता : पहले की फिल्मों में भी कहानी का महत्व था और आज भी है। एक अच्छी कहानी दर्शकों को हमेशा आकर्षित करती है।
2. भावनात्मक तत्व : दोनों दौर की फिल्मों में भावनात्मक तत्व प्रमुखता से दिखते हैं। प्यार, दोस्ती, परिवार और समाज जैसे मूल भावनात्मक विषय हमेशा फिल्म का हिस्सा रहे हैं।
3. गीत-संगीत : संगीत और गीत फिल्मों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। पहले की फिल्मों में भी संगीत को महत्वपूर्ण माना जाता था और आज भी गीत-संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है।
अंतर
1. तकनीकी विकास : पहले की फिल्मों में तकनीकी संसाधनों की कमी थी, जिससे विशेष प्रभाव (VFX) और ध्वनि गुणवत्ता में अंतर होता था। आज की फिल्मों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे दृश्य और ध्वनि में बहुत सुधार हुआ है।
2. कहानी की जटिलता : पहले की फिल्मों में सरल और सीधी कहानियाँ होती थीं, जबकि आज की फिल्मों में जटिल कथानक और विविधता देखी जाती है। आज की कहानियाँ अधिक वास्तविक और जमीनी होती हैं।
3. सामाजिक मुद्दे : पहले की फिल्मों में पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया जाता था, जबकि आज की फिल्मों में आधुनिक समाज के मुद्दों, जैसे महिला सशक्तिकरण, LGBTQ+ अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिया जाता है। आज की फिल्मे जैसे टायलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, थप्पड़, पिंक, क्वीन, छपाक जैसे फिल्मों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाया है।
4. अभिनय में अंतर : पहले की फिल्मों में अभिनय का तरीका बहुत नाटकीय होता था। दृश्यों और कहानी में भी नाटकीयता होती थी लेकिन कलाकार हर तरह की भूमिका करने में संकोच नही करते थे। पहले की फिल्मों स्टारडम नहीं होता था। आजकल की फिल्मों में अधिक स्वाभाविक और वास्तविक अभिनय की प्रवृत्ति तो है, लेकिन बहुत से कलाकार केवल खास रोल ही करना पसंद करते हैं। वह अपने स्टारडम से बाहर नहीं निकलना चाहते थे।
5. गीत-संगीत के स्तर में गिरावट : पहले की फिल्मों के गीत संगीत बेहद मधुर होते थे और गीतों का स्तर उत्कृष्ट कोटि का होता था। गीतों की भाषा शालीन और सभ्य होती थी तथा संगीत में बेहद मधुरता होती थी। पुरानी फिल्मों का गीत संगीत आज भी गुनगुनाया जाता है जबकि आज की फिल्मों के गीत संगीत में गिरावट आई है। गीतों में द्वि-अर्थी शब्दों और अश्लील शब्दों की भरमार होती है। संगीत भी बेहद भौंडा और शोर-शराबे वाला होता है। आज की फिल्मों के गीत-संगीत में से मधुरता गायब हो चली है।
6. सेंसरशिप और स्वातंत्रता : पहले की फिल्मों में सेंसरशिप का कड़ा नियंत्रण था और फिल्मों में कई विषयों पर बात करना कठिन था। आज की फिल्मों में विषयवस्तु पर अधिक स्वतंत्रता है और निर्माता विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं।
7. व्यापारिक दृष्टिकोण : पहले की फिल्मों में कला और कहानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जबकि आज की फिल्मों में व्यापारिक दृष्टिकोण और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महत्वपूर्ण हो गए हैं। बड़ी बजट की फिल्में और मार्केटिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
निष्कर्ष
पहले की फिल्मों में भावनात्मक गहराई और सरलता थी, जबकि आज की फिल्मों में तकनीकी उत्कृष्टता और विविधता है। दोनों ही दौर की फिल्मों का अपना महत्व और खूबसूरती है। पहले की फिल्में एक प्रकार की पारंपरिकता और सादगी लिए हुए होती थीं, जबकि आज की फिल्में आधुनिकता और जटिलता को दर्शाती हैं। दोनों ही अपने-अपने समय का प्रतिनिधित्व करती हैं और दर्शकों को मनोरंजन और विचार दोनों प्रदान करती हैं।
कक्षा में इस विषय पर चर्चा करते समय, दो या दो से अधिक विद्यार्थी दोनों दौर की फिल्मों के उदाहरण दे सकते हैं और उनसे उनके विचार पूछ सकते हैं कि वे किस प्रकार की फिल्मों को अधिक पसंद करते हैं और क्यों। इससे वे फिल्मों की विकास यात्रा और समाज पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
प्रश्न 2 : ‘तीसरी कसम’ जैसी और भी फ़िल्में हैं, जो किसी न किसी भाषा की साहित्यिक रचना पर बनी हैं। ऐसी फ़िल्मों की सूची निम्नांकित प्रपत्र के आधार पर तैयार करें।
| क्र. सं | फिल्म का नाम | साहित्यिक रचना | भाषा | रचनाकार |
| 1. | देवदास | देवदास | बंगला | शरत्चंद्र |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
उत्तर : कई साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में बनी है। ऐसी ही कुछ फिल्मों के नाम इस प्रकार है…
| क्र. सं | फिल्म का नाम | साहित्यिक रचना | भाषा | रचनाकार |
| 1. | देवदास | देवदास | बंगला | शरत्चंद्र |
| 2. | शतरंज के खिलाड़ी | शतरंज के खिलाड़ी | हिंदी | प्रेमचंद |
| 3. | नजराना | लक्ष्मण रेखा | हिंदी | गुलशन नंदा |
| 4. | झील के उस पार | झील के उस पार | हिंदी | गुलशन नंदा |
प्रश्न 3 : लोकगीत हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। तीसरी कसम’ फ़िल्म में लोकगीतों का प्रयोग किया गया है। आप भी अपने क्षेत्र के प्रचलित दो-तीन लोकगीतों को एकत्र कर परियोजना कॉपी पर लिखिए।
उत्तर : लोकगीत हमारे सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और यह हमारे रीति-रिवाजों, परंपराओं और जीवनशैली को दर्शाते हैं। ‘तीसरी कसम’ फिल्म में भी लोकगीतों का प्रयोग करके कहानी को और अधिक सजीव और प्रभावी बनाया गया है।
यहां आपके लिए कुछ प्रचलित लोकगीत प्रस्तुत किए जा रहें जो भारत के अलग-अलग राज्यों की लोक विरासत को प्रकट करते हैं…
1. बिहार का लोकगीत: ‘बिदेसिया’
बिदेसिया बिहार का एक प्रमुख लोकगीत है, जिसे विशेष रूप से छठ पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर गाया जाता है। यह गीत प्रायः प्रवासी मजदूरों के दर्द और उनके परिवारों की भावनाओं को दर्शाता है।
पिया जी सजनवा ए बिदेसिया
बिदेसी पिया जी सजनवा ए बिदेसिया
काहे सजनवा बिदेस गइले ओ बिदेसिया
ए बिदेसिया, बिदेसिया ए बिदेसिया
पिया जी सजनवा ए बिदेसिया
2. राजस्थान का लोकगीत: ‘केसरिया बालम’
केसरिया बालम राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अपने प्रियजन की वापसी का स्वागत करने के लिए गाया जाता है। यह गीत राजस्थान की संस्कृति और रंगीनता को दर्शाता है।
केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देस
केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देस
चाकी री चन्दन री गंध पधारो म्हारे देस
केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देस
3. महाराष्ट्र का लोकगीत: ‘लावणी’
लावणी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोकगीत है जो अपने तेज़ और जीवंत ताल के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत विशेष रूप से तमाशा और अन्य लोक नृत्यों में गाया जाता है।
पिंगळ्या पिंजऱ्यात सोन्याचा पिंजरा
उधळला मोगरा
चाफा बोलेना, चाफा चालेना
चाफा चालेना, चाफा बोलेना
परियोजना के लिए सुझाव
विद्यार्थी अपनी परियोजना कॉपी पर इन लोकगीतों को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके साथ ही, आप इन गीतों के बारे में संक्षिप्त परिचय, उनके महत्व और संबंधित सांस्कृतिक जानकारी भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो कुछ चित्र भी जोड़ सकते हैं जो इन गीतों को और आकर्षक बना देंगे।
परियोजना का स्वरूप इस प्रकार होगा..
1. शीर्षक: अपने क्षेत्र के प्रचलित लोकगीत
2. परिचय: लोकगीतों का महत्व और उनकी विशेषताएं
3. लोकगीत
– गीत का शीर्षक
– गीत के बोल
– गीत का महत्व और प्रसंग
इस प्रकार, विद्यार्थी अपनी परियोजना को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी संस्कृति के लोकगीतों को संरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं।
तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र : प्रहलाद अग्रवाल (कक्षा-10 पाठ-11 हिंदी स्पर्श 2) (NCERT Solutions)
कक्षा-10 हिंदी स्पर्श 2 पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठ
साखी : कबीर (कक्षा-10 पाठ-1 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
पद : मीरा (कक्षा-10 पाठ-2 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
मनुष्यता : मैथिलीशरण गुप्त (कक्षा-10 पाठ-3 हिंदी स्पर्श भाग 2) (हल प्रश्नोत्तर)
पर्वत प्रदेश में पावस : सुमित्रानंदन पंत (कक्षा-10 पाठ-4 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
तोप : वीरेन डंगवाल (कक्षा-10 पाठ-5 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
कर चले हम फिदा : कैफ़ी आज़मी (कक्षा-10 पाठ-6 हिंदी स्पर्श भाग-2) (हल प्रश्नोत्तर)
आत्मत्राण : रवींद्रनाथ ठाकुर (कक्षा-10 पाठ-7 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
बड़े भाई साहब : प्रेमचंद (कक्षा-10 पाठ-8 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
डायरी का एक पन्ना : सीताराम सेकसरिया (कक्षा-10 पाठ-9 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)
तताँरा-वामीरो की कथा : लीलाधर मंडलोई (कक्षा-10 पाठ-10 हिंदी स्पर्श 2) (हल प्रश्नोत्तर)